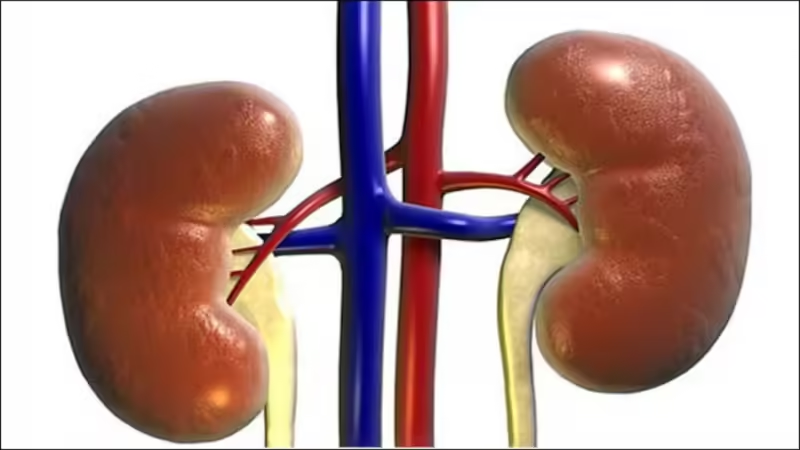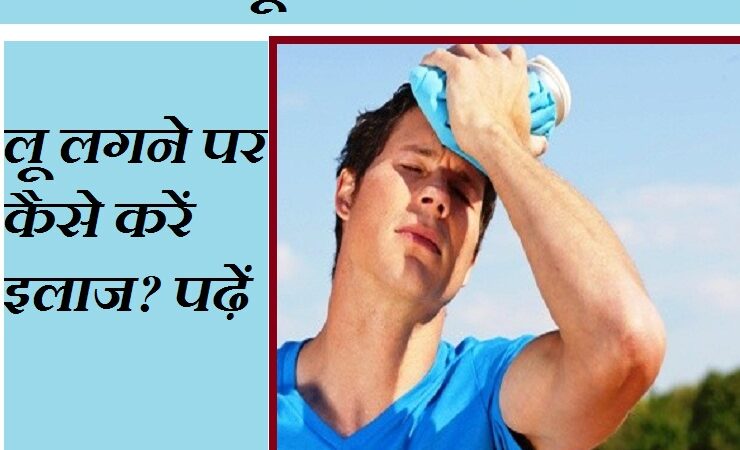कैंसर एक गंभीर और जटिल बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है।
कैंसर के प्रकार:
- फेफड़ों का कैंसर
- स्तन कैंसर (Breast Cancer)
- गर्भाशय कैंसर (Cervical Cancer)
- मुँह का कैंसर
- आंतों का कैंसर (Colorectal Cancer)
- त्वचा कैंसर (Skin Cancer)
- ब्लड कैंसर (Leukemia)
कैंसर होने के कारण:
- धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन
- अस्वास्थ्यकर खान-पान
- प्रदूषण और जहरीले रसायनों के संपर्क में आना
- अनुवांशिक कारण (परिवार में कैंसर का इतिहास)
- रेडिएशन और वायरस संक्रमण
लक्षण:
- शरीर में गाँठ या सूजन
- अचानक वजन घटना
- अत्यधिक थकान और कमजोरी
- लगातार खाँसी या गले में खराश
- घाव या अल्सर जो ठीक न हो
- असामान्य रक्तस्राव
कैंसर का इलाज:
- सर्जरी (Surgery) – कैंसर प्रभावित भाग को निकालना।
- कीमोथेरेपी (Chemotherapy) – दवाइयों के द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना।
- रेडियोथेरेपी (Radiotherapy) – रेडिएशन द्वारा कैंसर कोशिकाओं को खत्म करना।
- इम्यूनोथेरेपी (Immunotherapy) – शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना।
बचाव के उपाय:
- धूम्रपान और शराब से बचें।
- स्वस्थ आहार लें, जिसमें फल, सब्जियाँ और साबुत अनाज शामिल हों।
- नियमित व्यायाम करें।
- कैंसर की जल्द पहचान के लिए नियमित जाँच कराएं।
- सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाव करें
फेफड़ों का कैंसर (Lung Cancer)
फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें फेफड़ों की कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर (गाँठ) बना सकती हैं। यह कैंसर समय पर इलाज न मिलने पर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है।
फेफड़ों के कैंसर के प्रकार
- नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर (NSCLC) – यह सबसे आम प्रकार है और लगभग 85% मामलों में पाया जाता है।
- स्मॉल सेल लंग कैंसर (SCLC) – यह तेजी से फैलने वाला कैंसर है और ज्यादातर धूम्रपान करने वालों में पाया जाता है।
फेफड़ों के कैंसर के कारण
- धूम्रपान (तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट)
- पासिव स्मोकिंग (दूसरों के धुएँ के संपर्क में आना)
- वायु प्रदूषण और जहरीली गैसें
- रेडिएशन और रसायनों का संपर्क (जैसे एस्बेस्टस, आर्सेनिक)
- अनुवांशिक कारण (परिवार में कैंसर का इतिहास)
फेफड़ों के कैंसर के लक्षण
- लगातार खाँसी जो ठीक न हो
- खाँसी में खून आना
- सांस लेने में तकलीफ
- सीने में दर्द
- भूख न लगना और अचानक वजन घटना
- थकान और कमजोरी
फेफड़ों के कैंसर का निदान (Diagnosis)
- एक्स-रे और सीटी स्कैन – फेफड़ों में गाँठ या ट्यूमर का पता लगाने के लिए।
- बायोप्सी – फेफड़े की कोशिकाओं की जाँच के लिए।
- ब्रोंकोस्कोपी – फेफड़ों के अंदर कैमरे की सहायता से जाँच।
- पीईटी स्कैन – कैंसर की स्टेज का पता लगाने के लिए।
फेफड़ों के कैंसर का इलाज
- सर्जरी – प्रारंभिक अवस्था में कैंसर ग्रस्त भाग को हटाने के लिए।
- कीमोथेरेपी – कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं।
- रेडियोथेरेपी – उच्च ऊर्जा विकिरण से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है।
- इम्यूनोथेरेपी – शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए।
- टार्गेटेड थेरेपी – विशेष दवाइयों का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाया जाता है।
फेफड़ों के कैंसर से बचाव के उपाय
- धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दें।
- प्रदूषित हवा और रसायनों से बचाव करें।
- हेल्दी डाइट लें और नियमित व्यायाम करें।
- समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच कराते रहें
स्तन कैंसर (Breast Cancer)
स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर में से एक है, लेकिन यह पुरुषों को भी प्रभावित कर सकता है। इसमें स्तन की कोशिकाएँ असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और गाँठ (ट्यूमर) बना सकती हैं। यदि समय पर इलाज न मिले, तो यह शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है।
स्तन कैंसर के प्रकार
- इनवेसिव डक्टल कार्सिनोमा (IDC) – यह सबसे आम प्रकार है, जिसमें कैंसर स्तन की दुग्ध नलिकाओं (milk ducts) से निकलकर अन्य ऊतकों में फैल जाता है।
- इनवेसिव लोब्युलर कार्सिनोमा (ILC) – यह स्तन की ग्रंथियों (lobules) से शुरू होता है और अन्य भागों में फैल सकता है।
- डक्टल कार्सिनोमा इन-सिटू (DCIS) – यह कैंसर प्रारंभिक अवस्था में होता है और अभी तक अन्य ऊतकों में नहीं फैला होता।
- ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर (TNBC) – यह एक आक्रामक प्रकार का कैंसर होता है, जिसमें सामान्य हार्मोन रिसेप्टर्स नहीं होते, जिससे इसका इलाज चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
स्तन कैंसर के कारण और जोखिम कारक
- आनुवंशिकता – यदि परिवार में किसी को स्तन कैंसर हुआ हो, तो जोखिम बढ़ जाता है।
- हार्मोनल असंतुलन – एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के असंतुलन से खतरा बढ़ सकता है।
- उम्र बढ़ने के साथ जोखिम – 40 वर्ष के बाद स्तन कैंसर का खतरा अधिक होता है।
- अस्वास्थ्यकर जीवनशैली – धूम्रपान, शराब, और मोटापा बढ़ाने वाले आहार से खतरा बढ़ सकता है।
- रेडिएशन और हार्मोनल थेरेपी – अधिक रेडिएशन के संपर्क में आना और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना।
- बच्चों को स्तनपान न कराना – स्तनपान न कराने से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
स्तन कैंसर के लक्षण
- स्तन में गाँठ या सूजन
- निप्पल से असामान्य स्राव (खून या द्रव आना)
- स्तन या निप्पल का आकार या रंग बदलना
- निप्पल के चारों ओर लालिमा या दर्द
- अंडरआर्म (बगल) में गाँठ या सूजन
- त्वचा पर गड्ढे पड़ना (डिंपलिंग)
स्तन कैंसर की जाँच (Diagnosis)
- मेमोग्राफी – एक्स-रे की मदद से स्तन में किसी भी असामान्य वृद्धि की पहचान।
- अल्ट्रासाउंड और एमआरआई स्कैन – स्तन के ट्यूमर की स्थिति जानने के लिए।
- बायोप्सी – ट्यूमर के ऊतक का परीक्षण कर यह पता लगाना कि कैंसर है या नहीं।
- हार्मोन रिसेप्टर टेस्ट – यह देखने के लिए कि कैंसर हार्मोन-संवेदनशील है या नहीं।
स्तन कैंसर का इलाज
- सर्जरी
- लम्पेक्टोमी – केवल कैंसरयुक्त भाग को हटाया जाता है।
- मास्टेक्टोमी – पूरे स्तन को हटाया जाता है।
- कीमोथेरेपी – कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं।
- रेडियोथेरेपी – उच्च ऊर्जा विकिरण से कैंसर कोशिकाएँ नष्ट की जाती हैं।
- हॉर्मोन थेरेपी – यदि कैंसर हार्मोन-सम्बंधित हो तो यह थेरेपी दी जाती है।
- टार्गेटेड थेरेपी – कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाने के लिए विशेष दवाइयों का उपयोग किया जाता है।
स्तन कैंसर से बचाव के उपाय
- नियमित रूप से स्तन की स्वयं जाँच (Breast Self-Examination – BSE) करें।
- 40 वर्ष की उम्र के बाद हर साल मेमोग्राफी टेस्ट कराएं।
- संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें।
- धूम्रपान और शराब से बचें।
- बच्चों को स्तनपान कराएं, यह स्तन कैंसर के खतरे को कम कर सकता है
गर्भाशय कैंसर (Cervical Cancer & Uterine Cancer)
गर्भाशय कैंसर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है:
- सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) – यह गर्भाशय के निचले हिस्से (गर्भाशय ग्रीवा) में होता है।
- एंडोमेट्रियल कैंसर (Uterine Cancer) – यह गर्भाशय की अंदरूनी परत (एंडोमेट्रियम) में होता है।
1. सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer)
सर्वाइकल कैंसर के कारण
- ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) संक्रमण – यह सबसे बड़ा कारण है।
- असुरक्षित यौन संबंध और कई पार्टनर होना।
- कम उम्र में गर्भधारण और बार-बार प्रेग्नेंसी।
- धूम्रपान और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली।
- कमजोर इम्यून सिस्टम।
- अनुवांशिक कारण (यदि परिवार में किसी को यह कैंसर हो चुका है)।
सर्वाइकल कैंसर के लक्षण
- मासिक धर्म के बीच असामान्य रक्तस्राव।
- संभोग के बाद खून आना या दर्द होना।
- बदबूदार सफेद या भूरे रंग का योनि स्राव।
- कमर और पैरों में दर्द।
- पेशाब करने में जलन या दर्द।
सर्वाइकल कैंसर की जाँच (Diagnosis)
- पैप स्मीयर टेस्ट (Pap Smear Test) – प्रारंभिक अवस्था में कैंसर की पहचान के लिए।
- एचपीवी टेस्ट (HPV Test) – वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए।
- बायोप्सी – कैंसर कोशिकाओं की पुष्टि के लिए।
- कोलपोस्कोपी – गर्भाशय ग्रीवा की गहराई से जाँच।
सर्वाइकल कैंसर का इलाज
- सर्जरी – शुरुआती अवस्था में संक्रमित भाग को हटाया जाता है।
- रेडियोथेरेपी – रेडिएशन की मदद से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है।
- कीमोथेरेपी – दवाइयों द्वारा कैंसर कोशिकाओं को खत्म करना।
- इम्यूनोथेरेपी – शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए।
सर्वाइकल कैंसर से बचाव
- एचपीवी वैक्सीन (HPV Vaccine) 9 से 26 वर्ष की उम्र की लड़कियों को लगवानी चाहिए।
- नियमित रूप से पैप स्मीयर टेस्ट कराना।
- धूम्रपान और असुरक्षित यौन संबंध से बचना।
- संतुलित आहार और व्यायाम अपनाना।
2. एंडोमेट्रियल कैंसर (Uterine Cancer)
एंडोमेट्रियल कैंसर के कारण
- हार्मोन असंतुलन (एस्ट्रोजन का अधिक स्तर)।
- मोटापा और मधुमेह।
- 30 साल की उम्र के बाद बच्चा न होना।
- अनियमित मासिक धर्म।
- अनुवांशिक कारण।
एंडोमेट्रियल कैंसर के लक्षण
- रजोनिवृत्ति (Menopause) के बाद रक्तस्राव।
- मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव।
- पेट में सूजन और दर्द।
- अचानक वजन घटना।
- संभोग के दौरान दर्द।
एंडोमेट्रियल कैंसर की जाँच
- अल्ट्रासाउंड – गर्भाशय की परत की जाँच के लिए।
- एंडोमेट्रियल बायोप्सी – कैंसर कोशिकाओं की पुष्टि के लिए।
- एमआरआई और सीटी स्कैन – कैंसर की स्टेज जानने के लिए।
एंडोमेट्रियल कैंसर का इलाज
- सर्जरी (Hysterectomy) – पूरा गर्भाशय निकाल दिया जाता है।
- रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी।
- हार्मोन थेरेपी – एस्ट्रोजन के प्रभाव को कम करने के लिए।
एंडोमेट्रियल कैंसर से बचाव
- मोटापे पर नियंत्रण रखें।
- हार्मोन संतुलन बनाए रखें।
- नियमित व्यायाम करें।
- स्वस्थ आहार लें।
मुँह का कैंसर (Oral Cancer)
मुँह का कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें मुँह की कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर (गाँठ) बना सकती हैं। यह होंठ, जीभ, गाल, तालू, मसूड़े और गले को प्रभावित कर सकता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो यह कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है।
मुँह के कैंसर के कारण
1. तंबाकू और धूम्रपान:
- बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, पान मसाला, जर्दा आदि का सेवन।
- हुक्का और चबाने वाले तंबाकू उत्पादों से भी जोखिम बढ़ता है।
2. शराब का अधिक सेवन:
- अत्यधिक शराब पीने से मुँह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
3. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) संक्रमण:
- असुरक्षित यौन संबंधों से फैलने वाला यह वायरस भी मुँह के कैंसर का कारण बन सकता है।
4. खराब ओरल हाइजीन:
- गंदे दाँत और मसूड़े, बार-बार मुँह में छाले आना।
5. अधिक मसालेदार और गरम चीजें खाना:
- अधिक गरम चाय-कॉफी और मसालेदार भोजन से मुँह की कोशिकाओं को नुकसान पहुँच सकता है।
6. सूरज की किरणों का अधिक प्रभाव:
- होंठों के कैंसर का कारण बन सकता है।
मुँह के कैंसर के लक्षण
- मुँह के किसी भी हिस्से में गाँठ या सूजन।
- लम्बे समय तक मुँह के छाले न भरना।
- चबाने या बोलने में कठिनाई।
- मुँह के अंदर लाल या सफेद दाग।
- मुँह से असामान्य रक्तस्राव।
- मुँह का सुन्न पड़ना या कोई भाग सुन्न महसूस होना।
- अचानक वजन कम होना।
- कान में दर्द जो लंबे समय तक बना रहे।
मुँह के कैंसर की जाँच (Diagnosis)
बायोप्सी (Biopsy) – प्रभावित कोशिकाओं की जाँच की जाती है।
- एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई – कैंसर के फैलाव का पता लगाने के लिए।
- एंडोस्कोपी – मुँह और गले की आंतरिक स्थिति देखने के लिए।
मुँह के कैंसर का इलाज
1. सर्जरी (Surgery)
- कैंसर प्रभावित ऊतक को हटाने के लिए।
- अगर कैंसर बढ़ गया हो, तो जबड़े या जीभ का कुछ हिस्सा हटाना पड़ सकता है।
2. रेडियोथेरेपी (Radiotherapy)
- हाई-एनर्जी रेडिएशन से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है।
3. कीमोथेरेपी (Chemotherapy)
- दवाइयों के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को मारने का उपचार।
4. टार्गेटेड थेरेपी (Targeted Therapy)
- कैंसर कोशिकाओं को विशेष रूप से निशाना बनाकर खत्म करने की चिकित्सा।
मुँह के कैंसर से बचाव के उपाय
✅ तंबाकू और धूम्रपान छोड़ें।
✅ शराब का सेवन कम करें।
✅ संतुलित और पौष्टिक आहार लें।
✅ मुँह की सफाई का विशेष ध्यान रखें।
✅ सूरज की किरणों से बचने के लिए होंठों पर सनस्क्रीन लगाएँ।
✅ यदि मुँह में कोई असामान्य बदलाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
आंतों का कैंसर (Intestinal Cancer / Colorectal Cancer)
आंतों का कैंसर बड़ी आंत (Colon) और मलाशय (Rectum) में विकसित होने वाला एक गंभीर रोग है। इसे कोलोरेक्टल कैंसर भी कहा जाता है। यदि यह जल्दी पहचान में आ जाए, तो इसका इलाज संभव होता है।
आंतों के कैंसर के प्रकार
- कोलन कैंसर (Colon Cancer) – बड़ी आंत में होने वाला कैंसर।
- रेक्टल कैंसर (Rectal Cancer) – मलाशय (Rectum) में विकसित होने वाला कैंसर।
- स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर (Small Intestinal Cancer) – छोटी आंत में होने वाला कैंसर (यह दुर्लभ होता है)।
आंतों के कैंसर के कारण और जोखिम कारक
- गलत खान-पान – फाइबर की कमी, अधिक जंक फूड, तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड।
- मोटापा और शारीरिक गतिविधियों की कमी।
- धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन।
- आनुवांशिक कारण – परिवार में किसी को यह बीमारी हो तो जोखिम बढ़ सकता है।
- लंबे समय तक पेट संबंधी समस्याएँ – जैसे क्रोहन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस।
- बढ़ती उम्र – 50 वर्ष से अधिक उम्र में यह ज्यादा पाया जाता है।
आंतों के कैंसर के लक्षण
- पेट में लगातार दर्द या सूजन।
- कब्ज और दस्त का बार-बार होना।
- मल में खून आना या मल का रंग काला होना।
- अचानक वजन घटना और कमजोरी महसूस होना।
- भूख न लगना और थकान रहना।
- मल त्यागने के बाद भी पूरी तरह पेट साफ न होने का एहसास।
आंतों के कैंसर की जाँच (Diagnosis)
- कोलोनोस्कोपी (Colonoscopy) – बड़ी आंत की गहराई से जाँच करने के लिए।
- बायोप्सी (Biopsy) – कैंसर कोशिकाओं की पुष्टि के लिए।
- सीटी स्कैन और एमआरआई (CT Scan & MRI) – कैंसर की स्टेज जानने के लिए।
- सिग्मोइडोस्कोपी (Sigmoidoscopy) – मलाशय और बड़ी आंत के निचले हिस्से की जाँच के लिए।
- स्टूल टेस्ट (Stool Test) – मल में खून या कैंसर संबंधी संकेतों की जाँच।
आंतों के कैंसर का इलाज
1. सर्जरी (Surgery)
- कैंसर ग्रस्त आंत के हिस्से को हटाया जाता है।
- यदि कैंसर मलाशय तक फैल गया हो, तो स्टोमा (Stoma) बनाकर मल त्याग की प्रक्रिया बदली जा सकती है।
2. कीमोथेरेपी (Chemotherapy)
- कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं।
3. रेडियोथेरेपी (Radiotherapy)
- रेडिएशन की मदद से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है।
4. इम्यूनोथेरेपी (Immunotherapy)
- शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके कैंसर से लड़ने में मदद की जाती है।
5. टार्गेटेड थेरेपी (Targeted Therapy)
- विशेष दवाओं से कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाया जाता है।
आंतों के कैंसर से बचाव के उपाय
✅ फाइबर युक्त आहार खाएँ – फल, सब्जियाँ और साबुत अनाज का सेवन करें।
✅ प्रोसेस्ड और रेड मीट से बचें।
✅ नियमित व्यायाम करें और वजन नियंत्रित रखें।
✅ धूम्रपान और शराब से बचें।
✅ नियमित स्वास्थ्य जाँच कराएँ, खासकर यदि परिवार में किसी को यह बीमारी हो।
त्वचा कैंसर के प्रकार
- बेसल सेल कार्सिनोमा (Basal Cell Carcinoma – BCC)
- सबसे सामान्य प्रकार।
- यह धीरे-धीरे बढ़ता है और शरीर के अन्य हिस्सों में कम फैलता है।
- दिखने में मोती जैसे सफेद या गुलाबी रंग के उभरे हुए धब्बे।
- स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (Squamous Cell Carcinoma – SCC)
- यह अधिक आक्रामक होता है और फैल सकता है।
- लाल, खुरदुरे धब्बे, घाव या त्वचा पर गांठ के रूप में दिखता है।
- मेलानोमा (Melanoma) – सबसे खतरनाक प्रकार
- यह शरीर के अन्य भागों में तेजी से फैल सकता है।
- त्वचा पर काले या भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे दिखते हैं।
त्वचा कैंसर के कारण और जोखिम कारक
- सूरज की पराबैंगनी (UV) किरणें – लंबे समय तक धूप में रहने से खतरा बढ़ता है।
- टैनिंग बेड और लैम्प्स – कृत्रिम UV किरणें भी त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं।
- हल्की त्वचा (Fair Skin) – जिनकी त्वचा गोरी होती है, उन्हें अधिक खतरा होता है।
- आनुवांशिकता (Genetics) – यदि परिवार में किसी को त्वचा कैंसर हुआ हो, तो जोखिम बढ़ सकता है।
- कमजोर इम्यून सिस्टम – HIV या अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को अधिक खतरा होता है।
- बचपन में अधिक धूप जलन (Sunburns) – बार-बार धूप से झुलसने वाले लोगों को भविष्य में कैंसर हो सकता है।
त्वचा कैंसर के लक्षण
- नई गांठ, उभरी हुई त्वचा, या घाव जो ठीक नहीं हो रहा हो।
- त्वचा पर अनियमित आकार के भूरे, काले, गुलाबी, लाल, या सफेद धब्बे।
- मोल (तिल) का अचानक आकार, रंग या बनावट बदलना।
- खुजली, जलन या रक्तस्राव वाली त्वचा।
- त्वचा पर कठोर या खुरदरे धब्बे।
ABCDE नियम – त्वचा कैंसर की पहचान के लिए
- A (Asymmetry) – तिल या धब्बे का आकार असमान हो।
- B (Border) – किनारे अनियमित और असमान हों।
- C (Color) – धब्बे का रंग कई रंगों में बदले (काला, भूरा, लाल आदि)।
- D (Diameter) – आकार 6 मिमी से अधिक हो।
- E (Evolving) – धब्बे या तिल का आकार, रंग, या बनावट बदल जाए।
त्वचा कैंसर की जाँच (Diagnosis)
- डर्मेटोस्कोपी (Dermatoscopy) – त्वचा का माइक्रोस्कोप से परीक्षण।
- बायोप्सी (Biopsy) – कैंसर की पुष्टि के लिए ऊतक का सैंपल लिया जाता है।
- सीटी स्कैन / एमआरआई (CT Scan / MRI) – उन्नत चरण में कैंसर के फैलाव का पता लगाने के लिए।
त्वचा कैंसर का इलाज
1. सर्जरी (Surgery)
- कैंसरग्रस्त ऊतक को हटाने के लिए।
- यदि कैंसर गहरा हो, तो अधिक ऊतक हटाने पड़ सकते हैं।
2. मोस सर्जरी (Mohs Surgery)
- त्वचा कैंसर के छोटे-छोटे हिस्से निकालकर माइक्रोस्कोप से जाँच की जाती है।
3. क्रायोथेरेपी (Cryotherapy)
- कैंसर कोशिकाओं को ठंडे तरल नाइट्रोजन से जमाकर नष्ट किया जाता है।
4. कीमोथेरेपी (Chemotherapy)
- यदि कैंसर फैल गया है, तो दवाओं से इलाज किया जाता है।
5. रेडियोथेरेपी (Radiotherapy)
- रेडिएशन किरणों से कैंसर कोशिकाओं को खत्म किया जाता है।
6. इम्यूनोथेरेपी (Immunotherapy)
- शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए।
त्वचा कैंसर से बचाव के उपाय
✅ सूरज की किरणों से बचाव करें – सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में कम जाएँ।
✅ सनस्क्रीन (SPF 30 या अधिक) लगाएँ – खासकर बाहर जाने से 30 मिनट पहले।
✅ पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें – हल्के, सूती कपड़े और टोपी का उपयोग करें।
✅ टैनिंग बेड और UV लैंप से बचें।
✅ नियमित रूप से त्वचा की जाँच करें – यदि कोई असामान्य बदलाव दिखे, तो डॉक्टर से संपर्क करें।
त्वचा कैंसर के प्रकार
- बेसल सेल कार्सिनोमा (Basal Cell Carcinoma – BCC)
- सबसे सामान्य प्रकार।
- यह धीरे-धीरे बढ़ता है और शरीर के अन्य हिस्सों में कम फैलता है।
- दिखने में मोती जैसे सफेद या गुलाबी रंग के उभरे हुए धब्बे।
- स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (Squamous Cell Carcinoma – SCC)
- यह अधिक आक्रामक होता है और फैल सकता है।
- लाल, खुरदुरे धब्बे, घाव या त्वचा पर गांठ के रूप में दिखता है।
- मेलानोमा (Melanoma) – सबसे खतरनाक प्रकार
- यह शरीर के अन्य भागों में तेजी से फैल सकता है।
- त्वचा पर काले या भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे दिखते हैं।
त्वचा कैंसर के कारण और जोखिम कारक
- सूरज की पराबैंगनी (UV) किरणें – लंबे समय तक धूप में रहने से खतरा बढ़ता है।
- टैनिंग बेड और लैम्प्स – कृत्रिम UV किरणें भी त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं।
- हल्की त्वचा (Fair Skin) – जिनकी त्वचा गोरी होती है, उन्हें अधिक खतरा होता है।
- आनुवांशिकता (Genetics) – यदि परिवार में किसी को त्वचा कैंसर हुआ हो, तो जोखिम बढ़ सकता है।
- कमजोर इम्यून सिस्टम – HIV या अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को अधिक खतरा होता है।
- बचपन में अधिक धूप जलन (Sunburns) – बार-बार धूप से झुलसने वाले लोगों को भविष्य में कैंसर हो सकता है।
त्वचा कैंसर के लक्षण
- नई गांठ, उभरी हुई त्वचा, या घाव जो ठीक नहीं हो रहा हो।
- त्वचा पर अनियमित आकार के भूरे, काले, गुलाबी, लाल, या सफेद धब्बे।
- मोल (तिल) का अचानक आकार, रंग या बनावट बदलना।
- खुजली, जलन या रक्तस्राव वाली त्वचा।
- त्वचा पर कठोर या खुरदरे धब्बे।
ABCDE नियम – त्वचा कैंसर की पहचान के लिए
- A (Asymmetry) – तिल या धब्बे का आकार असमान हो।
- B (Border) – किनारे अनियमित और असमान हों।
- C (Color) – धब्बे का रंग कई रंगों में बदले (काला, भूरा, लाल आदि)।
- D (Diameter) – आकार 6 मिमी से अधिक हो।
- E (Evolving) – धब्बे या तिल का आकार, रंग, या बनावट बदल जाए।
त्वचा कैंसर की जाँच (Diagnosis)
- डर्मेटोस्कोपी (Dermatoscopy) – त्वचा का माइक्रोस्कोप से परीक्षण।
- बायोप्सी (Biopsy) – कैंसर की पुष्टि के लिए ऊतक का सैंपल लिया जाता है।
- सीटी स्कैन / एमआरआई (CT Scan / MRI) – उन्नत चरण में कैंसर के फैलाव का पता लगाने के लिए।
त्वचा कैंसर का इलाज
1. सर्जरी (Surgery)
- कैंसरग्रस्त ऊतक को हटाने के लिए।
- यदि कैंसर गहरा हो, तो अधिक ऊतक हटाने पड़ सकते हैं।
2. मोस सर्जरी (Mohs Surgery)
- त्वचा कैंसर के छोटे-छोटे हिस्से निकालकर माइक्रोस्कोप से जाँच की जाती है।
3. क्रायोथेरेपी (Cryotherapy)
- कैंसर कोशिकाओं को ठंडे तरल नाइट्रोजन से जमाकर नष्ट किया जाता है।
4. कीमोथेरेपी (Chemotherapy)
- यदि कैंसर फैल गया है, तो दवाओं से इलाज किया जाता है।
5. रेडियोथेरेपी (Radiotherapy)
- रेडिएशन किरणों से कैंसर कोशिकाओं को खत्म किया जाता है।
6. इम्यूनोथेरेपी (Immunotherapy)
- शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए।
त्वचा कैंसर से बचाव के उपाय
✅ सूरज की किरणों से बचाव करें – सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में कम जाएँ।
✅ सनस्क्रीन (SPF 30 या अधिक) लगाएँ – खासकर बाहर जाने से 30 मिनट पहले।
✅ पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें – हल्के, सूती कपड़े और टोपी का उपयोग करें।
✅ टैनिंग बेड और UV लैंप से बचें।
✅ नियमित रूप से त्वचा की जाँच करें – यदि कोई असामान्य बदलाव दिखे, तो डॉक्टर से संपर्क करें।
ब्लड कैंसर (Blood Cancer / Leukemia, Lymphoma, Myeloma)
ब्लड कैंसर शरीर में खून बनाने वाली प्रणाली को प्रभावित करता है। यह अस्थि मज्जा (Bone Marrow), रक्त कोशिकाओं और लिम्फेटिक सिस्टम में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है।
ब्लड कैंसर के प्रकार
- ल्यूकेमिया (Leukemia)
- जब रक्त में सफेद रक्त कोशिकाएँ (WBCs) अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाती हैं।
- यह बच्चों और वयस्कों दोनों में हो सकता है।
- लिम्फोमा (Lymphoma)
- जब लिम्फोसाइट्स (प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएँ) असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं।
- यह मुख्य रूप से लिम्फ नोड्स (Lymph Nodes) और लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है।
- मायलोमा (Myeloma)
- यह प्लाज्मा कोशिकाओं (Plasma Cells) को प्रभावित करता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है।
ब्लड कैंसर के कारण और जोखिम कारक
- आनुवांशिक कारण (Genetic Mutations) – परिवार में किसी को कैंसर होने पर जोखिम बढ़ सकता है।
- रेडिएशन और केमिकल्स का संपर्क – अत्यधिक रेडिएशन या बेंजीन जैसे केमिकल्स के संपर्क में आना।
- वायरल संक्रमण – जैसे एचटीएलवी-1 (HTLV-1) और एपस्टीन-बार वायरस (EBV)।
- कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली – एचआईवी या अन्य रोगों से पीड़ित लोगों को अधिक खतरा।
- धूम्रपान और शराब – ये डीएनए को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
ब्लड कैंसर के लक्षण
- लगातार बुखार या संक्रमण।
- अचानक वजन कम होना और कमजोरी महसूस होना।
- शरीर में खून की कमी (एनीमिया)।
- हड्डियों और जोड़ों में दर्द।
- गले या बगल में लिम्फ नोड्स (गाँठ) का बढ़ना।
- बार-बार नाक से खून आना या खून जमने में कठिनाई।
- पसीना अधिक आना, खासकर रात में।
ब्लड कैंसर की जाँच (Diagnosis)
- ब्लड टेस्ट (CBC Test) – रक्त में असामान्य कोशिकाओं की पहचान के लिए।
- बोन मैरो बायोप्सी (Bone Marrow Biopsy) – अस्थि मज्जा में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए।
- लिम्फ नोड बायोप्सी (Lymph Node Biopsy) – लिम्फोमा की पुष्टि के लिए।
- सीटी स्कैन और एमआरआई (CT Scan & MRI) – कैंसर के फैलाव की जाँच के लिए।
- इम्यूनोफेनोटाइपिंग और जेनेटिक टेस्टिंग – कैंसर की विशेषताओं को समझने के लिए।
ब्लड कैंसर का इलाज
1. कीमोथेरेपी (Chemotherapy)
- कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है।
2. रेडियोथेरेपी (Radiotherapy)
- उच्च ऊर्जा विकिरण (Radiation) से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है।
3. बोन मैरो ट्रांसप्लांट (Bone Marrow Transplant / Stem Cell Therapy)
- अस्थि मज्जा में स्वस्थ स्टेम सेल प्रत्यारोपित की जाती हैं।
- ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट – मरीज के अपने स्टेम सेल का उपयोग।
- एलोजेनिक ट्रांसप्लांट – डोनर से लिए गए स्टेम सेल का उपयोग।
4. इम्यूनोथेरेपी (Immunotherapy)
- शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके कैंसर से लड़ने में मदद की जाती है।
5. टार्गेटेड थेरेपी (Targeted Therapy)
- दवाइयाँ कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाकर नष्ट करती हैं।
ब्लड कैंसर से बचाव के उपाय
✅ धूम्रपान और शराब से बचें।
✅ स्वस्थ आहार लें – हरी सब्जियाँ, फल और एंटीऑक्सिडेंट युक्त भोजन करें।
✅ रेडिएशन और हानिकारक केमिकल्स से बचाव करें।
✅ नियमित रूप से स्वास्थ्य जाँच कराएँ।
✅ व्यायाम करें और वजन संतुलित रखें।